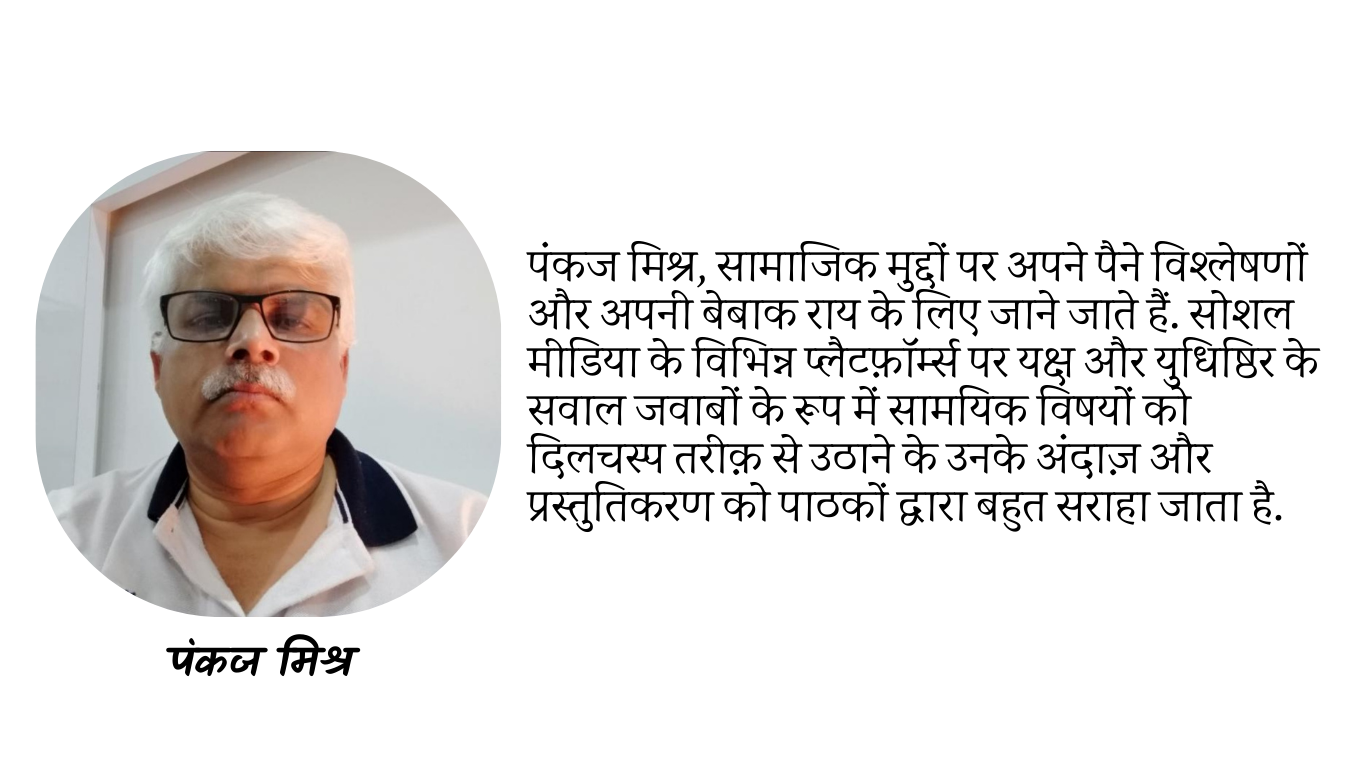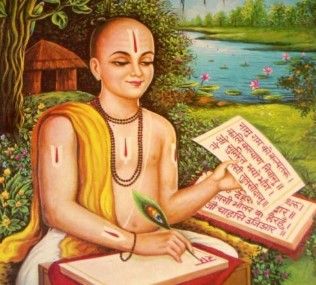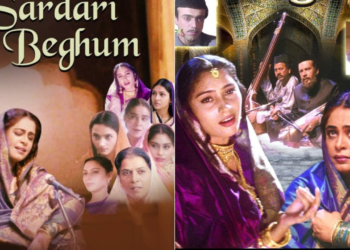एक साहित्यिक कृति कितनी प्रभावशाली हो सकती है, उसका चरम बिंदु है राम चरित मानस. दूजा ऐसा उदाहरण नहीं है. पर क्या आपने कभी सोचा कि कब रामचरित मानस पुस्तकालय से उठ कर, हमारे घर के पूजा स्थलों तक आ गई? यूं तो सामाजिक मुद्दों के विश्लेषक पंकज मिश्र का यह आलेख पुराना है, राम जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले का है, लेकिन इसमें मौजूद मुद्दे इसे हमेशा सामयिक बनाए रखेंगे. अत: बहुत ज़रूरी है कि हम सभी इसे पढ़ें और इसमें मौजूद सवालों के ईमानदार जवाब सोचें, क्योंकि कई बार, कई सवालों के जवाब हमें संयुक्त रूप से बेहतरी की ओर ले जाते हैं/ले जाने का माद्दा रखते हैं.
रामचरित मानस के तमाम पात्रों के बारे में हमारा जितना सामान्य ज्ञान है या उनके प्रति जो भी भाव है, उसके एकमेव निर्माता हैं गोस्वामी तुलसी दास और एकमात्र सन्दर्भ ग्रन्थ है राम चरित मानस. ज्ञात रहे तुलसी अकबर के शासनकाल में यह रचना कर रहे थे.
राम कथा बहुत पुरानी है. ज़ाहिर है, तुलसी भी उसी कथा से प्रेरित हुए होंगे. राम कथा के अनेक संस्करण हैं, पात्रों का चरित भी विभिन्न आख्यानों में भिन्न-भिन्न हैं, परंतु हम हिंदी पट्टी के लोग उन तमाम चरित को वैसा ही जानते मानते हैं, जैसा तुलसी दास ने बताया.
यानी रामचरित का मान्य नैरेटिव तुलसी दास का ही सेट किया हुआ है. तुलसी जहां चुप हैं, वहां हम सब चुप हैं और किसी विमर्श में अगर कोई उसका दूसरा पाठ प्रस्तुत करता है तो हम या तो विवाद करते है या आहत हो कर दुःखी अथवा भाषिक रूप से हिंसक हो उठते है. एक साहित्यिक कृति कितनी प्रभावशाली हो सकती है उसका चरम बिंदु है राम चरित मानस. दूजा ऐसा उदाहरण नहीं है.
मानस, जो एक कथा की काव्यात्मक पुनर्प्रस्तुति भर है, परंतु इतनी प्रभावी है कि हम न केवल उनके नायकों को भगवान का दर्जा देते हैं, बल्कि खलनायकों को परमानेंट दुष्ट और मानव द्रोही मान लेते हैं. चाहे फिर हज़ारों वर्षों में युगधर्म या युगीन सत्य बदल चुका हो, मगर यह बदलाव उनके विमर्श में अकाउंट फ़ॉर नहीं होता. तुलसी का पात्र चित्रण काल निरपेक्ष हो चुका है.
दिलचस्प यह भी है कि उन पात्रों को हम न केवल दिव्य मानते हैं, बल्कि ऐतिहासिक भी मानते हैं. अब विडम्बना यह कि इतिहास के चरित्रों के रूप में यदि उनका मूल्यांकन हो, तब हमारी भावनाएं आहत होती हैं और उन्हें दिव्य किरदार मानने से हमारा इतिहास बोध आहत होता है. अब दुविधा ये है कि एक समझदार आदमी करे तो क्या करे?
मुझे लगता है तुलसी को यदि ज़रा भी यह आभास होता कि उनका भक्ति महाकाव्य लोक के बीच में इस रूप में पैठेगा कि उनके तमाम रूपक अभिधा में समझे जाएंगे, उनके तमाम पात्र ऐतिहासिक सत्य का रूप धारण कर कालान्तर में समाज में विग्रह और सत्ता प्राप्ति का औज़ार बन जाएंगे तो वह एक डिस्क्लेमर ज़रूर डालते.
यह ठीक है कि साहित्यकार दूर तक और भीतर तक देख लेता है, लेकिन वह भी एक हद से आगे नही देख सकता. तुलसी भी इसके अपवाद नहीं हो सकते.
देश काल बदला, युग धर्म बदला, एक साहित्यिक कृति का धार्मिक इस्तेमाल होने लगा. राम चरित मानस पुस्तकालय से निकल कर पूजा घर में पहुंच गया. मानस के साहित्यिक मूल्यांकन की बजाय उसे अगरबत्ती दिखाई जाने लगी, उसका अखंड पाठ होने लगा. ठेके पर कीर्तनिए बुलाए जाने लगे. यह जानना भी दिलचस्प होगा कि मानस के अखंड पाठ की परंपरा कब शुरू हुई.
मानस, पहले मस्तिष्क से च्युत हुआ तो हृदयस्थ हुआ, फिर हृदय से च्युत हुआ तो कंठस्थ हो गया. च्युत होते होते मानस के पात्र चैनलों में आ गए और कमर्शल ब्रेक के मोहताज हो गए, सड़क पे आ गए और नारों में समा गए. कहां तो वह संस्कृति में होते थे वहां से साहित्य में आए , फिर धर्म का हिस्सा बने और आज राजनीति के औज़ार हो गए. उनकी क्रिया और कर्तव्यों के बजाय जाति पर विमर्श होने लगा. उनसे मुकदमा लड़वाया जाने लगा और आज तुलसी के भगवान इंसान में रिड्यूस होकर फ़ैज़ाबाद की लोअर कोर्ट में एक मुकदमे के फ़रीक़ बन गए हैं. किसी बाबर या मीर बाक़ी में इतनी ताक़त नहीं हो सकती, यह धतकर्म तो पतित राजनीति ही कर सकती थी.
तुलसी होते तो अपनी सार्वकालिक महत्वपूर्ण रचना पर रो रहे होते, क्योंकि तुलसी भक्त पहले थे कवि बाद में और दोनों बहुत बड़े थे.
अब तो रामलला मुकदमा जीत चुके हैं. उनके वक़ील ने न जाने कितनी बार मी लॉर्ड कहा होगा और उसे सुन सुन कर राम जी, लीला करते हुए कितनी बार भन्नाए भी होंगे. कितनी बार सोचा होगा कि इसे अपना विराट स्वरूप दिखा ही दूं कि असली लॉर्ड तो मैं हूं, मगर फिर मुकदमे की याद आ गई होगी कि कहीं जज साहेबान बुरा न मान जाएं.
फ़ोटो: पिन्टरेस्ट