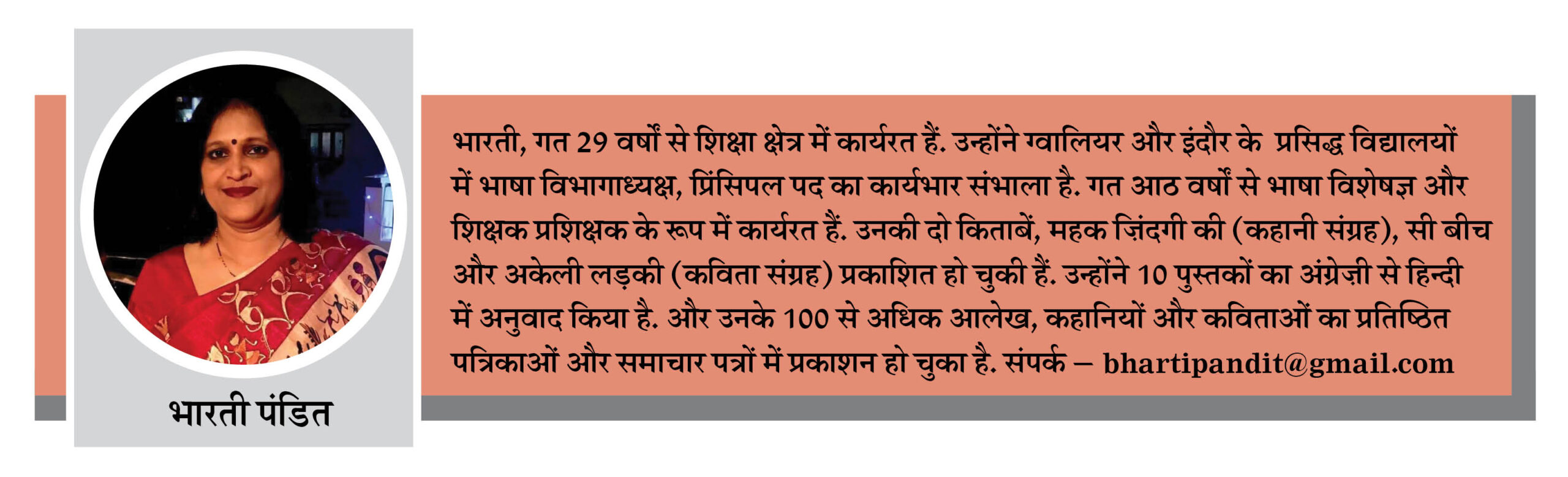बड़े दिनों बाद बड़े परदे पर अमिताभ और नीना गुप्ता जैसे नामी सितारें देखकर फ़िल्म देखने जाने का मन तो बनेगा ही न! फिर बड़े अख़बारों के रिव्यू भी ठीकठाक ही थे तो लगा फ़िल्म देख ही लेनी चाहिए. पर ढाई घंटे की बेहद धीमी गति से चलती फ़िल्म ने कुछ ख़ास प्रभावित नहीं किया, यह भी समझ में आया कि यदि स्क्रीन प्ले ठीक न हो तो नामी सितारे भी कुछ ख़ास कर नहीं पाते. फ़िल्म गुड बाय को देखने के बाद भारती पंडित की पहली प्रतिक्रिया यही है. यदि आप भी इस फ़िल्म को देखने और ना देखने के बीच कहीं झूल रहे हैं तो उनकी लिखी यह पूरी समीक्षा पढ़ें.
फ़िल्म: गुड बाय
सितारे: अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता, रश्मिका मंदाना, एली अवराम अन्य.
डायरेक्टर: विकास बहल
रन टाइम: 142 मिनट
फ़िल्म की कहानी है आज के परिवारों जैसे ही चंडीगढ़ में रहने वाले हरीश भल्ला के परिवार की, जहां बच्चे अपनी-अपनी दुनिया में मस्त हैं, माता-पिता से अनचाहे ही दूरियां कायम हो चली हैं। ग़ुस्सैल और कड़क पिता वैसे भी बच्चों को रुचते नहीं, बस मां यानी गायत्री ही है, जिसके प्यार और ज़िन्दादिली ने सबको एक कच्चे से सूत्र में बांध रखा है. इस परिवार के तीन अपने बच्चे हैं– तारा, नकुल और करण और एक गोद लिया हुआ बेटा अंगद…इसके अलावा घर में काम करने वाली लड़की को भी गायत्री ने बचपन से अपने पास रखा है. एक रात अचानक गायत्री की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है.
फ़िल्म शुरू होती है हरीश भल्ला की बेटी तारा भल्ला जो अपने दोस्त मुदस्सर के साथ मुंबई में लिव इन में रहती है, की पहला केस जीतने की पार्टी से. धमाल पार्टी है, म्यूज़िक, मस्ती, दारू और धमाल सब कुछ है… तभी फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, फ़ोन बार टेंडर के पास चार्जिंग के लिए लगा दिया जाता है। पार्टी ख़त्म होती है, सुबह बार टेंडर फ़ोन देने आता है. बताता है कि ढेर सारे कॉल्स आए थे…उतने में हरीश भल्ला का फ़ोन आता है, जो एक बहस पर ही ख़त्म होता है, तारा ग़ुस्से में फ़ोन काट देती है…तब दरवाज़े पर खड़ा बार टेंडर बताता है कि रात को तारा की मां का देहांत हो गया है और उसके पिताजी यही बताने के लिए बार-बार फ़ोन कर रहे थे. पिताजी के साथ किए गए अपने व्यवहार पर तारा को अफ़सोस होता है…वह झटपट फ़्लाइट पकड़ कर चंडीगढ़ चल पड़ती है. इसी तरह करण और अंगद भी अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालकर चंडीगढ़ पहुंचते हैं. नकुल मां की इच्छा का पालन करने हाईकिंग पर गया है अतः उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है.
हरीश भल्ला ख़ुद को संयत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उन्हें बराबर यह लगता है कि गायत्री के जाने से किसी को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा है और इसे लेकर उनके मन में भारी रोष है. वास्तव में हम दुनिया को अपनी ही नज़र से देखते हैं मगर यह सच है कि शोक मनाने का या ख़ुशी मनाने का हरेक का तरीक़ा एक सा नहीं हो सकता, कुछ लोग शोक में खाना-पीना छोड़ देते हैं तो कुछ लोग शोक में ज़्यादा खाते हैं…दूसरी बात यह भी कि मौत के बाद ज़िंदगी में वापस आना अपरिहार्य है, और उस पर भी पेट भरने का इंतज़ाम करना सबसे पहली प्राथमिकता है. शायद शोक वाले घर में चूल्हा न जलाने की प्रथा भी उस घर के सदस्यों की मानसिक अवस्था को देखते हुए उन्हें इस काम से मुक्त रखने की मंशा से बनाई गई होगी, पर क्या इसे ही ब्रह्म सत्य माना जाना चाहिए?
फ़िल्म में भारतीय परिवेश में मौत के बाद जो रीति-रिवाज़ किए या करवाए जाते हैं, उनको दिखाने की कोशिश की गई है, मृत शरीर का रख-रखाव भी पंडित के कहने के मुताबिक़ ही किया जा रहा है…किस दिशा में शव रखा जाएगा, क्या-क्या सामग्री लगेगी यह सब. तारा इस सबसे इत्तेफ़ाक नहीं रखती, वहीं हरीश का मानना है कि यह सब क्रियाकर्म आवश्यक है, करण का मानना है कि क्या फ़र्क़ पड़ता है यदि समाज के लिए यह सब कर भी लिया तो.

हमारे समाज में जन्म से ज्यादा मुश्क़िल मौत की है, जहां मरने वाला तो अपनी इच्छा बताए बिना चल पड़ता है मगर पीछे रह गए लोग हरेक क्रियाकर्म को सिर्फ़ लोग क्या कहेंगे या आत्मा भटकेगी इसी डर से इच्छा-अनिच्छा से पूरा करते हैं…एक दृश्य में इस सबका विरोध करते हुए तारा कहती है, ‘आपने कभी मां से पूछा कि उन्हें कैसे जाना था? आज मां होती तो यह सब उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता.’
मौत पर आमतौर पर होने वाले सामाजिक दिखावे को भी प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, पर फिर भी कोई भी बात गहरे से छूती नहीं है, झकझोरती नहीं है. हां, शोक व्याप्त है तो आंसू आ ही जाते हैं. मां की मौत के ही बहाने सारा परिवार अरसे बाद एक साथ है. कुछ तकरार है, आपसी मतभेद हैं, गिले-शिकवे हैं, पर फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, सब साथ हैं.
मुझे इस फ़िल्म में अंत तक यह समझ में नहीं आया कि निर्देशक विकास बहल कहना क्या चाहते हैं? कथा कहन का भी एक तरीक़ा होता है, या तो तथ्यों-घटनाओं को ज्यों का त्यों दर्शकों के सामने रख दिया जाए और दर्शकों को ही उसका सार निकालने दिया जाए, या फिर शुरुआत से ही एक स्टैंड लेते हुए कहानी को आगे बढ़ाया जाए.
ढाई घंटे की इस फ़िल्म में शुरुआती हिस्से में तो ऐसा लगता है कि विकास बहल मौत के नाम पर समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करना चाहते हैं, ध्यान दिलाना चाहते हैं. तारा का विरोध और अन्य बातें इसी के सन्दर्भ में समझ में आ रही थीं मगर आख़िर तक जाते-जाते वे यह स्थापित करते नज़र आते हैं कि सारे कर्मकांड एकदम सही हैं, चाहे पिंड दान हो, या मृत्यु भोज हो या कौए में के रूप में मृत व्यक्ति की आत्मा का घर आना हो.
इस बात से एकदम इत्तेफ़ाक है कि जो बात हमें समझ में नहीं आतीं या जो दिखाई नहीं देती वह होती नहीं हैं या सही नहीं हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर एक तथ्य यह भी है कि कुछ बातें सार्वभौमिक हैं और कुछ समुदायों द्वारा बनाई हुई. इनके बीच में भेद समझना बहुत ही आवश्यक है. फ़िल्म बड़ी मुश्क़िल तब पैदा करती है जब तारा जैसी तार्किक और जागरूक लड़की अंत में यह मान लेती है कि कौए के रूप में उसकी मां ही आई है. कहां ले जाना चाहते हैं हम अपनी सोच को? एक जागरूक और तर्कशील लड़की को अन्धविश्वासी लड़की के रूप में रूपांतरित होते दिखाने में क्या समझदारी है भला? ऐसे ही अंत में करण और नकुल का अचानक बाल कटाने का निर्णय हैरान करता है, यहां भी तर्क छोड़कर भावना का आसरा लिया गया लगता है.
अभिनय की बात करें तो नीना गुप्ता सारा श्रेय लूट ले गईं. हरेक फ्रेम को बेहतरीन तरीक़े से जीया है उन्होंने. अमिताभ भी अभिनय में ख़ासे अच्छे लगे हैं, कुछ फ्रेम में तो बहुत ही स्मार्ट लगे हैं. बाक़ी जिसके हिस्से जितना काम आया, सभी ने ईमानदारी से किया.
सुनील ग्रोवर भी पंडित की भूमिका में अच्छे लगे हैं. हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के समय अमिताभ के एकल संवाद वाला सीन अजीब सा लगा, इसकी एडिटिंग भी गड़बड़ है. इसी तरह पतंग वाला दृश्य भी एकदम बेमेल सा लगता है. हरीश के सत्तरवें जन्मदिन वाला अंतिम दृश्य अच्छा लगा है.
फ़िल्म का अधिकतर हिस्सा घर में ही फ़िल्माया गया है, अतः फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ख़ास था नहीं. अमित त्रिवेदी ने संगीत पर ख़ासा काम किया है. माई री और जयकाल-महाकाल गीत बढ़िया बन पड़े हैं. हिचकी वाला पहला गीत अब हर पार्टी में धमाल करने वाला है.
कुछ बातें जो इस फ़िल्म में अच्छी लगीं- मृत्यु सत्य है और इस सत्य को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें, उतना ही बेहतर होता है. वास्तव में मृत्यु राईट टर्न है, व्यक्ति चलता रहता है, बस हमारी आंखों से ओझल हो जाता है. हर व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि उसे विदाई किस तरह से लेनी है, ठीक उसी तरह जैसे वह यह तय करता है कि उसे जन्मदिन कैसे मनाना है. मुश्क़िल यही है कि हमारे समाज में हम हर उस बात पर बात करने से बचते हैं, जो हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, फिर चाहे वह मौत हो, प्रेम हो, सेक्स हो या हिंसा हो. बहरहाल, यदि थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं तो ओटीटी पर देखिएगा, हां यदि वेल्ले बैठे हैं और समय काटना ही है तो देख आइए एक बार.
फ़ोटो: गूगल