तय तो ये किया था कि कुछ दिन फ़िल्मों से दूरी बरतना है पर कल रात एक चिरसंचित स्वप्न पूरा होने की रात थी. जी हां, कल रात मैंने ‘दस्तक’ देखी. शायद लम्बे अरसे से अपने ज़ेहन पर हो रही दस्तक को नज़रअंदाज़ न कर सकी. इस फ़िल्म को बेदी साहब का शानदार शाहकार कहने में मुझे तनिक भी झिझक महसूस नहीं होती. फ़िल्म की अनकन्वेंशनल कहानी और सिचुएशन्स कमाल हैं!
दस्तक राजिंदर सिंह बेदी की फ़िल्म है. उन्ही का स्क्रीन प्ले और निर्देशन भी. यह उनकी पहली फ़िल्म थी, जो उन्हीं के रेडियो प्ले ‘नक़्ल-ए-मकानी’ पर आधारित थी. राजिंदर सिंह बेदी की फ़िल्मों में पात्रों से कहीं अधिक परिस्थितियों की अहम भूमिका होती है, दस्तक भी अपवाद नहीं है. कहानी शुरू होती है एक नवविवाहित जोड़े हामिद (संजीव कुमार) और सलमा (रेहाना सुल्ताना) के एक मोहल्ले में आकर घर लेने से. प्रेम में आकंठ डूबा यह जोड़ा अपना आशियाना बसाने आता है तो बहुत शुक्रगुज़ार महसूस करता है कि उन्हें मुम्बई में कम क़ीमत पर एक ऊपरी मंज़िल पर बना दो कमरों का फ़्लैटनुमा घर मिल गया है. साथ में एक अदद पलंग भी. रात गाने का आलाप सुनकर सलमा चौंकती है तो हामिद उसे तसल्ली देता है कि ‘वो जगह’ यहां से कुछ दूर है.
उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं कि जिस मकान में वे रहने आए हैं वह अब से कुछ ही समय पहले तक एक मशहूर तवायफ़ शमशाद बानो (मशहूर कव्वाल शकीला बानो भोपाली) की रिहाइश था. करेला ऊपर नीम चढ़ा ये कि सलमा ख़ुद एक गायक परिवार से ताल्लुक़ रखती है और उसके वालिद, ताज़दार साहब एक समय के मशहूर कव्वाल रह चुके हैं. उसके पास सुरीला गला ही नहीं है, बल्कि साथ आते हुए वह अपना तानपुरा भी साथ लाई है. थकान उतारते हुए प्रथम एकांत में सलमा, हामिद को राग चारुकेशी पर आधारित एक बंदिश सुनाती है, ‘बहिया न धरो ओ बलमा’. गाना सुनते ही मोहल्ले वालों के कान खड़े हो जाते हैं. बस यहीं से शुरू होता बदनाम मोहल्ले में उस मकान के उनके दरवाज़े पर अवांछित, अनामंत्रित दस्तकों का सिलसिला, जो उनका चैन और सुकून दोनों छीन लेता है. दोनों के बीच प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी दोनों के बीच हालात की दुश्वारियां अपनी जगह बनाने लगती हैं. पहली रात में संगीत के दिव्य जादू में डूबे हामिद को गाने और तानपुरे के ज़िक्र से भी नफ़रत होने लगती है.
मकान दिलाने वाला पानवाला (अनवर हुसैन), मोहल्ले में सक्रिय दलाल, पड़ोस के दो जवान लड़के और उस मकान पर कभी भी आ टपकने वाले शमशाद बानो के ग्राहक, सब मिलकर इस दम्पति का जीना हराम कर देते हैं. सबका फ़ायदा इसी में है कि सीधी सादी गृहस्थिन सलमा भी पेशा शुरू कर दे. नए मकान का मिलना बहुत मुश्क़िल है इस पर परिस्थितियां लगातार बिगड़ती चली जाती हैं. दोनों कुछ दिनों के लिये गांव भी जाते हैं, पर ताज़दार साहब (निरंजन शर्मा) की ख़राब माली हालत उन्हें वापिस इसी जहन्नुम में ला पटकती है. हामिद, जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है, अपने ज़मीर से जूझने लगता है. अंत बहुत ही अप्रत्याशित और मार्मिक है.
इस फ़िल्म को बेदी साहब का शानदार शाहकार कहने में मुझे तनिक भी झिझक महसूस नहीं होती. फ़िल्म की अनकन्वेंशनल कहानी और सिचुएशन्स कमाल हैं. कभी प्रेमातुर पति तो कभी ग़ुस्सैल खाविंद, संजीव कुमार तो हमेशा की तरह हैं ही लाजवाब और डेब्यू हीरोइन के तौर रेहाना सुल्तान भी कम प्रभावित नहीं करतीं. फ़िल्म की शुरुआत में एक शरारती प्रेममयी खिलंदड़ बीवी और बाद में एक बन्द घर में हर रोज़ एक नई मुसीबत से जूझती परेशान औरत दोनों ही रूपों में रेहाना ने अपना असर छोड़ा है. हैरत है कि बोल्ड फ़िल्मों के ठप्पे ने हमसे एक हुनरमंद और बेहतरीन अभिनेत्री को छीन लिया. छोटी सी भूमिकाओं में मनमोहन कृष्ण (सहृदय पड़ोसी बुजुर्ग), अंजू महेंद्रू (हामिद के ऑफ़िस में स्टेनो), निरंजन शर्मा भी प्रभाव छोड़ने में सफल रहे हैं. मक्कार पानवाले की भूमिका में अनवर हुसैन ख़ूब जमे हैं, वहीं गाना सुनने आए सेठ की भूमिका में कमल कपूर की भाव भंगिमाओं को देखकर पाकीज़ा याद गई, लगा वे शौक़ीन मिज़ाज रईस के रोल में क्या ख़ूब जमते हैं. अपनी ढल गई जवानी के चलते सलमा को अपने रंग ढंग में ढल जाने को उतारू शमशाद की भूमिका में शकीला बानो भोपाली मुझे बार बार श्यामा की याद दिला रही थीं.
फ़िल्म का एक बेहतरीन और मुख्य पात्र है- इसका कालजयी संगीत. अतिश्योक्ति न होगी अगर कहा जाए कि मदनमोहन साहब को अमर बना देने वाली फ़िल्मों में दस्तक का मक़ाम सबसे ऊपर है. संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान के साथ उन्होंने भी इस फ़िल्म के लिये नैशनल अवॉर्ड अपने नाम किया था. इससे भी बड़ा अवॉर्ड था इसके संगीत को मिली बेपनाह मुहब्बत, जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिल में घर बनाए हुए है. बहिया न धरो ओ बलमा, माई री मैं कासे कहूं (लता), तुमसे कहूं एक बात परों सी हल्की हल्की (लता), हम हैं मता-ए-कूंचा-ओ-बाज़ार की तरह (लता) यानी हर गाना एक बेशक़ीमती हीरा. माई री मैं कासे कहूं का मेल वर्शन जो मदनमोहन साहब की आवाज़ में है और जिसे मैंने सबसे अधिक बार सुना है, फ़िल्म में नहीं मिला. शायद इसकी रेकॉर्डिंग सिर्फ़ ऐल्बम के लिए हुई थी.
‘मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह….’ जी हां मजरूह साहब की मौसिकी ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है इन नग़मों के रूप में. इस फ़िल्म से ऋषिकेश मुखर्जी भी जुड़े हुए थे, फ़िल्म एडिटर के रूप में. फ़िल्म के डायलॉग शानदार हैं, जो स्क्रीन प्ले के साथ शायद बेदी साहब ने ही लिखे. कुछ सीन बेहद उम्दा बन पड़े हैं. जैसे ख़ाली पिंजरे के दोनों ओर खड़े हामिद और सलमा की चुहल भूलना मुश्क़िल है. एक डायलाग याददाश्त के आधार पर लिख रही हूं, शब्दों से अधिक भावों पर ध्यान दीजिए, तभी सलमा अपने गांव के मुंहबोले हिन्दू भाई के हवाले से कहती है, पिंजरे में पंछी रखना पाप है. हामिद जवाब देता है, बाहर छोड़ देना भी तो पाप है, बाहर जाने कितने बाज़, शिकरे घूम रहे हैं, कब झपट्टा मार लें. यहां सांकेतिक तौर पर पंछी की नहीं सलमा अपनी बात कर रही है और हामिद का इशारा भी बाहर पेश आनेवाले खतरों की ओर है.
एक अन्य दृश्य में फेंके गए पत्थरों से खिड़की का कांच टूट जाने पर सलमा कहती है, परेशानी ये है कि मुझे सांस आने लगी, मुझे सांस लेने की आदत नहीं है. ये डायलॉग इतना मार्मिक है और उस पर दोनों के एक्सप्रेशन्स, सीधे स्मृतियों में जज़्ब होने लायक सीन है. पाली गई मैना की क़ैद से बन्द मकान में अपनी क़ैद की तुलना करती सलमा गांव जाते समय उसे भी आज़ाद कर देती है. कुछ और दृश्य हैं, जो लंबे समय तक अपने होने की याद दिलाते रहेंगे, पर उन्हें देखने के लिए आपको ये फ़िल्म देखनी होगी.
फ़िल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है और इसके गाने आज ज़रूर सुनिएगा. इसका संगीत सीधे रूह में उतर जाने की ताब रखता है और हिंदी सिनेमा की कालजयी फ़िल्मों की मेरी सूची ‘दस्तक’ के बिना अधूरी है. क्या मालूम आप भी यही महसूस करें.
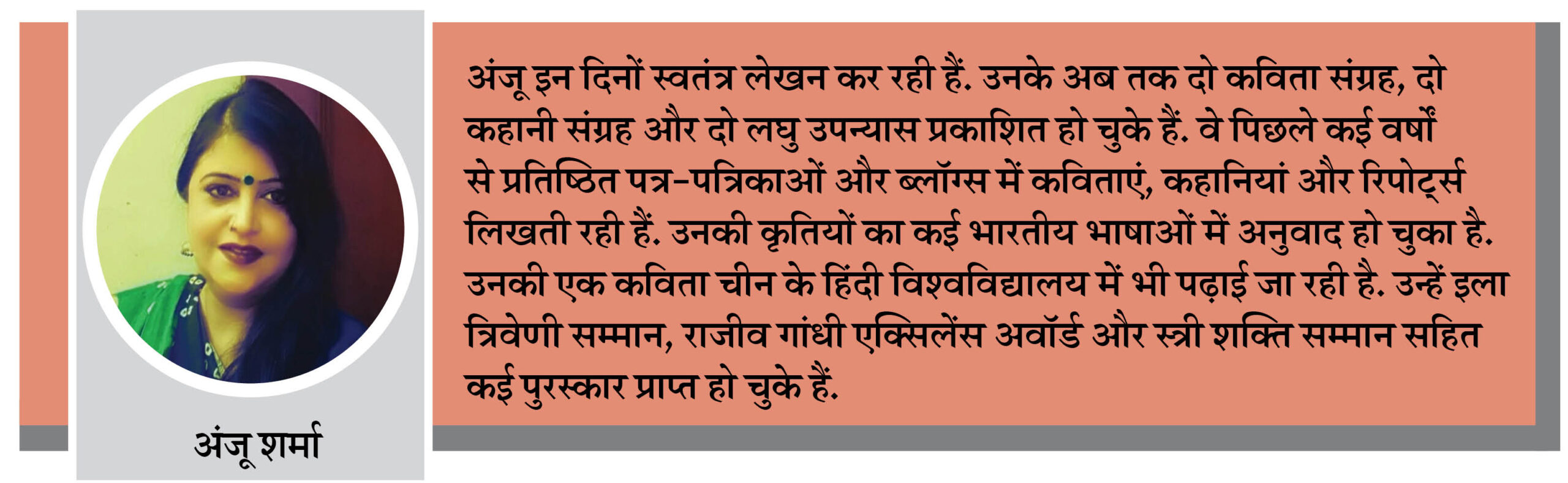
फ़ोटो: गूगल








