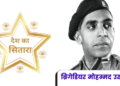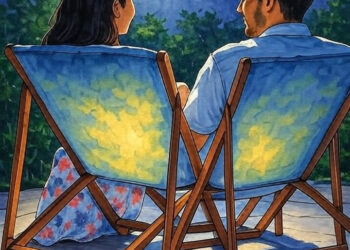साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई न कोई हिंदी फ़िल्म सिने पर्दे पर न पहुंचती हो. इनमें से कुछ सफल रहती हैं तो कुछ असफल. कुछ दर्शकों को कुछ अर्से तक याद रह जाती हैं, कुछ को सिनेमाघर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं. लेकिन जब कोई फ़िल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फ़िल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी क़ामयाब रहती है. ऐसी ही एक कालजयी फ़िल्म है राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका वाली फ़िल्म तीसरी कसम. हिंदी फ़िल्मों के इतिहासकार प्रह्लाद अग्रवाल फ़िल्म तीसरी कसम की कहानी बता रहे हैं.
फ़िल्म: तीसरी कसम
कलाकार: राज कपूर, वहीदा रहमान, दुलारी, इफ़्तेख़ार और अन्य
निर्देशक: बासु भट्टाचार्य
कहानी: फणीश्वरनाथ रेणु
गीत: शैलेन्द्र और हसरत जयपुरी
संगीत: शंकर-जयकिशन
एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फ़िल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति ‘तीसरी कसम’ उर्फ़ ‘मारे गए गुलफाम’ को सिने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई. आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फ़िल्मों में की जाती है. इस फ़िल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई बल्कि इसमें अपने ज़माने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फ़िल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन ऐक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया. फ़िल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने
भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी. इस मायने में एक यादगार फ़िल्म होने के बावजूद ‘तीसरी कसम’ को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फ़िल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फ़िल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फ़िल्म
बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है.
‘संगम’ की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उन्होंने एक साथ चार फ़िल्मों के निर्माण की घोषणा की,‘मेरा नाम जोकर’, ‘अजन्ता’, ‘मैं और मेरा दोस्त’ और ‘सत्यम् शिवम् सुंदरम्’. पर जब 1965 में राज कपूर ने ‘मेरा नाम जोकर’ का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उन्होंने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फ़िल्म का एक ही भाग बनाने में छह वर्षों का समय लग जाएगा. इन छह वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फ़िल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन् 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की ‘तीसरी कसम’ भी शामिल है. यह वह फ़िल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की. यही नहीं, ‘तीसरी कसम’ वह फ़िल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सैल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा. ‘तीसरी कसम’ फ़िल्म नहीं, सैल्यूलाइड पर लिखी कविता थी.

‘तीसरी कसम’ शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फ़िल्म है. ‘तीसरी कसम’ को ‘राष्ट्रपति स्वर्णपदक’ मिला, बंगाल फ़िल्म जर्नलिस्ट असोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया. मास्को फ़िल्म फेस्टिवल में भी यह फ़िल्म पुरस्कृत हुई. इसकी कलात्मकता की लंबी-चौड़ी तारीफें हुईं. इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है. उन्होंने ऐसी फ़िल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि-हृदय ही बना सकता था. शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं.
राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फ़िल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर. शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास ‘तीसरी कसम’ की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया. पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले,‘‘मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा.’’ शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर ज़िंदगी-भर की दोस्ती का ये बदला देंगे. शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुसकराते हुए कहा,“निकालो एक रुपया, मेरा पारिश्रमिक! पूरा एडवांस.’’ शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं, फिर अब शैलेंद्र तो फ़िल्म-निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे. राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फ़िल्म की असफलता के ख़तरों से आगाह भी किया. पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्म-संतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी.

‘तीसरी कसम’ कितनी ही महान फ़िल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्क़िल वितरक मिले. बावजूद इसके कि ‘तीसरी कसम’ में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर-जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी और इसके गीत भी फ़िल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फ़िल्म को ख़रीदने वाला कोई नहीं था. दरअसल इस फ़िल्म की संवेदना किसी दो से चार बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी. उसमें रची-बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी. इसीलिए बमुश्क़िल जब ‘तीसरी कसम’ रिलीज़ हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ. फ़िल्म कब आई, चली गई, मालूम ही नहीं पड़ा.
ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र बीस सालों तक फ़िल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर-तरीक़ों से नावाकिफ़ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे. ‘श्री 420′ का एक लोकप्रिय गीत है,‘प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यूं डरता है दिल.’ इसके अंतरे की एक पंक्ति,’रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां’ पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की. उनका ख़याल था कि दर्शक ‘चार दिशाएं’ तो समझ सकते हैं,’दस दिशाएं’ नहीं. लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए. उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए. कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे. और उनका यक़ीन ग़लत नहीं था. यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए. शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया. उनके गीत भाव-प्रवण थे-दुरूह नहीं. ‘मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे. शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए. यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फ़िल्म के द्वारा भी साबित किया था.
‘तीसरी कसम’ यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फ़िल्मों में से है जिन्होंने साहित्य-रचना के साथ शत-प्रतिशत न्याय किया हो. शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को ‘हीरामन’ बना दिया था. हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका. और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी ‘हीराबाई’ ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था. कजरी नदी के किनारे उकडू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है ‘मन समझती हैं न आप?’ तब हीराबाई जुबान से नहीं, आंखों से बोलती है. दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते. ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी,’तीसरी कसम’. अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान,’चलत मुसाफ़िर मोह लियो रे पिंजड़े
वाली मुनिया.’ टप्पर-गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते-गाते बच्चों का हुजूम,‘लाली-लाली डोलिया में लाली रे दुलहनिया’, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान! अभावों की ज़िंदगी जीते लोगों के सपनीले कहकहे.
हमारी फ़िल्मों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, लोक-तत्त्व का अभाव. वे ज़िंदगी से दूर होती है. यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफ़ाई किया जाता है. दुख का ऐसा वीभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके. और ‘तीसरी कसम’ की यह ख़ास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में, जीवन-सापेक्ष प्रस्तुत करती है.
मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं, कवि कहा है. वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन-लिप्सा से कोसों दूर थे. जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी. उनके गीतों में सिर्फ़ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत
अपनी मंज़िल तक पहुंचा जाता है. व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है.

शैलेंद्र ने ‘तीसरी कसम’ को अपनी भावप्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया. मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है-सजनवा बैरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई बांचै भाग न बांचै कोय… अभिनय के दृष्टिकोण से ‘तीसरी कसम’ राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फ़िल्म है. राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला-मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, ‘तीसरी कसम’ में मासूमियत के चर्मोत्कर्ष को छूते हैं. अभिनेता राज कपूर जितनी ताक़त के साथ ‘तीसरी कसम’ में मौजूद हैं, उतना ‘जागते रहो’ में भी नहीं. ‘जागते रहो’ में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन ‘तीसरी कसम’ वह फ़िल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता. वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है. खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ़ दिल की ज़ुबान समझता है, दिमाग़ की नहीं. जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं. बहुत बड़ी बात यह है कि ‘तीसरी कसम’ राज कपूर के अभिनय-जीवन का वह मुकाम है, जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे. उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था. लेकिन ‘तीसरी कसम’ में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है. वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु ख़ुद हीरामन में ढल गया है. हीराबाई की फेनू-गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी ‘मनुआ-नटुआ’ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक-सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है. ‘तीसरी कसम’ की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी. कहानी का रेशा-रेशा, उसकी छोटी-से-छोटी बारीकियां फ़िल्म में पूरी तरह उतर आईं.